ब्लॉगिंग में छुआछूतः बद से बदतर भला?
कथादेश में अविनाश के कॉलम पर अपनी राय लिखी पर समय पर पोस्ट करने से चूक गया। चुंकि अब कमेंटियाकर कुछ लाभ नहीं अतः इस पोस्ट का ही नाजायज लाभ उठाया जा रहा है।
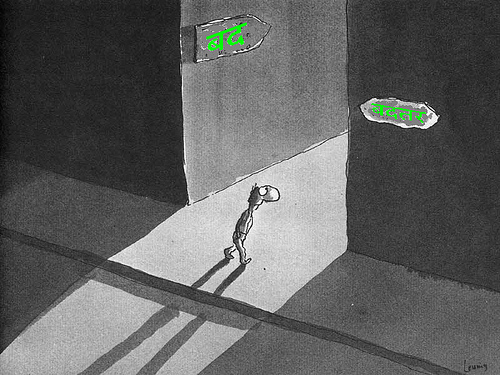
नारद काँड के बाद से बारंबार चिट्ठाजगत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात उठ रही हैं। बेवजह ही सही पर चिंताजनक बात है, क्योंकि ब्लॉग खुली खरी बात कहने के ही माध्यम हैं। पर मुझे इन नारों में केवल संघर्ष का ही पुट दिखता है। नारद के विवाद के समय ये गीकी और साधारण चिट्ठाकारों का संघर्ष था (जो कुछ कुछ अब भी जारी है, मसलन “इन्होंने मंटो और चुगताई को नहीं पढ़ा इसलिये अश्लील भाषा की पहचान में अक्षम हैं”) और भड़ास के बाद ये साधारण ब्लॉगारों और अभिजात्य ब्लॉगरों में लट्ठम लट्ठ बन चुका है। और इस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है।
कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे चिट्ठाकारी में एक तरह की “छुआछूत की पैठ बन पड़ी है, या जातिय महासभायें बन रही हैं”, पर भाषा का मसला कृपया ना उछालें, छूआछूत इस पर तो कतई नहीं है। ये पृथकतावाद है नारद वालों और मुहल्ले वालों के बीच। “नारद वाले” कौन हैं ये कोई नहीं जानता पर इनसे “पोस्ट मुहल्ला” ब्लॉगियों को सख्त परहेज़ है। मुहल्ले पर चढ़े ब्लॉगरोल को देख कर आप “जात बाहर” चिट्ठाकारों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस सूची में मेरा चिट्ठा तो खैर होने लायक ही नहीं था पर फुरसतिया, जीतेंद्र और रवि रतलामी का भी नहीं है। और फुरसतिया तो गीकी तमगा भी नहीं लगाते।
तो अविनाश और नीलिमा भड़ास के समर्थन में उठ खड़े हुये हैं ये नकारते हुये कि ना ना कर के भी मेरे जैसे अनेक भड़ास नियमित रूप से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ज़ाहिर तौर पर प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। नीलिमा ने बद और बदतर में बदतर को चुनना उचित समझा है, पहले गीकी, और अब कथित अभिजात्य चिट्ठाकारों को मुँह चिढ़ाने के लिये। अविनाश शायद भड़ास से जुड़े लोगों की संख्या से प्रभावित हैं, ऐसी ही संख्या वे मुहल्ला पर देखना चाहते थे, और यहाँ भी वे सत्य नकार रहे हैं कि संख्या में अंतर ज्यादा क्यों है, उन्होंने कभी इंटरनेट पर पॉर्न और इरॉटिक लेखन के बाजार पर तव्वजोह नहीं दिया। उन्हें भड़ास एक नया आंदोलन लग रहा है। पर ये आंदोलन एनडीटीवी या उन अखबारों में क्यों नहीं है जिनसे अविनाश या भड़ास के लेखक जुड़े हैं? अलहदा माध्यम? संपादकीय नियंत्रण? अविनाश ब्लॉग की परिभाषा तो ठीकठाक लिखते हैं, “संपादकीय पाश से मुक्ति”, तो ये मुक्ति कैसी है? भड़ास की भाषा होली वाली है तो क्या हम इंटरनेट पर रोज होली मनायें, क्योंकि ये हमारा घर, आफिस या हमारा समाज नहीं है? और अगर रोज़ मनाना है तो मेरा सवाल परंपरागत मीडिया से जुड़े इन लोगों से ये है कि हम आपके मीडिया में इस परीक्षण को क्यों ना दुहरायें? आप के अपने आफिशीयल मीडिया, या खरी कहें तो रोजी रोटी के ज़रिये, में ये “साहस” कहाँ और क्यों छुपा बैठा है? कथनी और करनी में ये अंतर क्यों?
इसके बावजूद आप भड़ास पर यशवंत के संपादकीय नियंत्रण के पुट देख सकते हैं, और ये कोई कमी नहीं है बल्कि एक जिम्मेवार प्रकाशन का परिचायक है। “नीलिमा को भड़ास की हेडमिस्ट्रेस बनाने” के हास्य में ये इच्छा छुपी है कि भड़ास में कीचड़ कम न हो क्योंकि ये हमारे मन में छुपे शूकर के यदा कदा लोट लगाने में सहायक होता है। ये अजीब जिद है, किसी श्याने स्कूली बच्चे जैसी जो अपने उपद्रवी साथी को खिड़की के काँच तोड़ने को उकसाये सिर्फ इसलिये कि उससे ये पत्थर उछाला नहीं जाता। इच्छा यही है तो मैं वाकई हिन्दी पॉर्न ब्लॉग का इंतज़ार करुंगा।
क्या मुझे आप बुद्धिजीवियों को ये बार बार समझाना होगा कि जहाँ कोई औपचारिक नियामक, कोई सेंसर नहीं है या हो नहीं सकता वहाँ तो सेल्फ सेंसरशिप या स्वनियामन और भी ज़रूरी हो जाता है। इसमें कोई गला घोंटने वाली बात नहीं है, ये वैसी ही बात है कि जब ड्राइंगरूम में देर शाम मित्रों और जाम के साथ खुली छूट बात हो रही हो तो पत्नी और बच्चे को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता है। ये उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात है, जैसा किसी ने लिखा था कि “आप की लहराती छड़ी की स्वतंत्रता की हद वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरु होती है”।
मुझे लगता है कि ये तबका ये सोचता है कि पहले मुहल्ले और फिर भड़ासियों के लेखन से इंटरनेटिय लेखन को “कल्चर शॉक” लगा है। ये बात निहायत हास्यास्पद है क्योंकि अव्वल तो ब्लागिंग के पहले नेट पर हिन्दी में पर्याप्त लेखन था ही नहीं और दूसरे, कि इंटरनेट पर पॉर्न तब से है जब से लोग इंटरनेट क्या है ये जानने लगे। इस लेखन से कोई शॉक वॉक किसी को नहीं लगा, जब रिक्शे और सब्ज़ी वाले हमारी पत्नियों के गुजरते बेपरवाह माँ भैन करते हैं तो वे इसे अनुसुना कर चलते जाने की आदि हैं। भड़ास भी करेगा तो जिसे पढ़ना है पढ़ेगा जिसे अनसुना करना है करेगा। पर जिस तरह हम अपनी बहन और पत्नी को कलारी के नज़दीक से न गुजरने की सलाह देते हैं वही सलाह हम भड़ास के मामले में भी देने लगेंगे। इतनी सी बात है। यूट्यूब ग्राफिक विडियो संपादित कर देता, हटा देता है, मेटाकैफे उन्हें सॉफ्ट पॉर्न के स्तर तक जाने देता है। अलग अलग मंच है, अलग अलग आचारनीति। क्या यूट्यूब पर आजादी का हनन हो रहा है? ये साबित करना चाहते हैं कि ये नया आंदोलन लाये हैं, पर मेरा मानना है कि ये कोई नीयो-ब्लॉगिंग नहीं है, क्योंकि हिन्दी ब्लॉगिंग ही नीयो है। अभी तो ये दिशायें तलाश रहा है, फैल सिकुड़ कर आकार ले रहा है तो किस पैमाने पर माप रहे हैं आप इसे? जैसे जैसे लेखन बढ़ रहा है इसकी छटा भी निखर रही है। किस लेखन को कैसा पाठक मिले ये आप क्यों तय करते हैं? नारद नहीं दिखाता भड़ास की पोस्ट, न दिखाये, जिसे पढ़ना होगा सीधे ब्लॉग पर पढ़ लेगा। आप घर में मुजरा क्यों देखना चाहते हैं, मुजरा जहाँ होता है वहाँ जाकर देखें। कौन रोकता है?
अप्रेल 2004 में लिखी एक पोस्ट में मुझे “साले” शब्द लिखने में भी संकोच हो रहा था। आज शायद अपशब्द भी बेखटके लिख सकूं। ये महज़ तीन साल के विकास(?) का प्रतिफल है। अविनाश को जो भाषा होली वाली लगी वो एक समय पर मुझे अनूप शुक्ल के ब्लॉग की लगी थी जब उन्होंने शुरुवात की थी अपने चिट्ठे की। यह और कुछ नहीं इवाल्विंग चिट्ठाकारी का स्वरूप है। जब मामला ही विचाराधीन है तो अभी इस पर फैसले कैसे सुनाये जा सकते हैं?


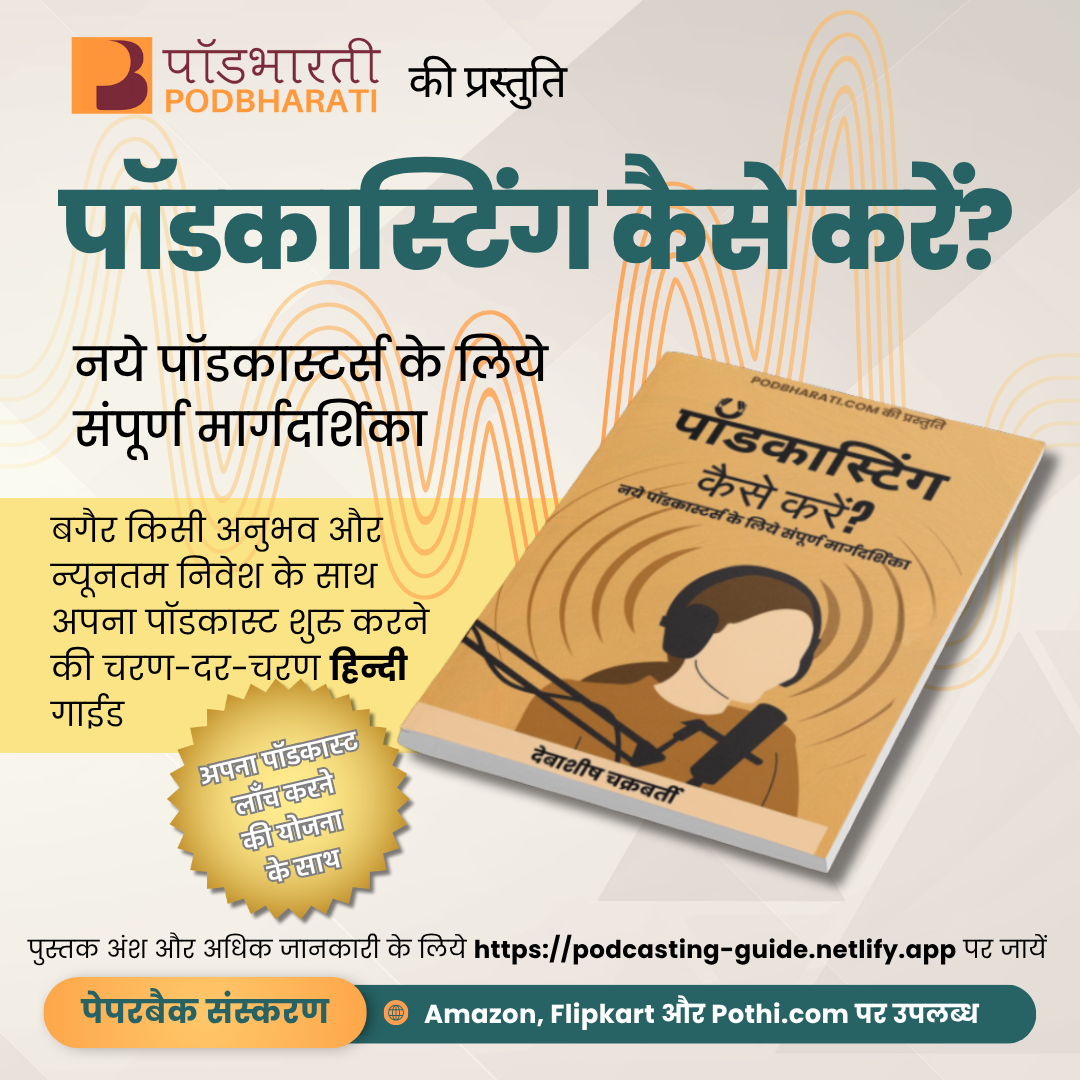

फ़ैसले सुनाने का सवाल ही नहीं है, पर आपकी गाथा सुंदर है, सुविचारित है। हम तो बस कह रहे हैं कि इस नई बनती दुनिया में घर और बाहर का विभेद न करें। न नारद ज़रूरी है, न ब्लॉगवाणी। ज़रूरी हमेशा वो बात होगी, जो कही जाएगी। आपकी भी, हमारी भी और उनकी भी, जो दरअसल बेआवाज़ हैं। हां, लेकिन आपकी वो गुज़ारिश या अपील या कहें दलील बेकार-बेमतलब है, जब आप कहते हैं कि आप जहां पेशेवर तौर पर जुड़े हैं, वहां इस तरह की मांग या इस तरह की भाषा या इस तरह की अभिव्यक्ति की मुहिम क्यों नहीं चलाते। नहीं चलाते इसलिए क्योंकि पहले भी ये मैं साफ कर चुका हूं कि अभिव्यक्ति के तमाम पारंपरिक साधनों में जिस तरह के पुराने जड़ हालात हैं, उसमें ब्लॉगिंग एक हथियार की तरह है, जिसका इस्तेमाल वही कर रहा है, जिसके हाथ लग रहा है। हां, मैं आपका लिंक अभी डाल रहा हूं। आप भले नामोल्लेख में भी नीलिमा का लिंक डालने के साथ हमारा लिंक डालना भूल जाएं।
बहुत खूब देबाशीष जी, मज़ा आया। मुद्दे बिल्कुल साफ है।
व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि भडास निकालने का हक सबको है मगर भाषा का भदेस…उस पर तो जिम्मेदारी से सोचना चाहिए। यह मानना संकुचित बुद्धि दर्शाएगा कि भड़ास तो भदेस भाषा में ही उजागर होती है। ऐसा नहीं है। भड़ास के बावजूद आपकी वाणी पर बुद्धि का अंकुश लगा है इसीलिए आपने अपना मंच बनाया है। खामख्वाह साहसी कहलाने के लिए मुंहजोरी या भदेस की शरण लेने में कोई तुक नहीं। फिलहाल तो हिन्दी में भदेस के समर्थन या विरोध में किसी आंदोलन की गुजाइश नहीं है, आवश्यकता भी नहीं।
आपके विचार पसंद आए. धन्यवाद!
आपने कुच्छ कायदे की बात की है. बडी जुतम पैजार हो रही है. शायद कुछ फ़र्क आये.
इस लेख में आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये है. इन पर अभी काफी दिनों तक विचार विमर्श चलेगा. उम्मीद है कि यह चर्चा स्वस्थ तरीके से आगे बढेगी.
हां, हिन्दी चिट्ठाजगत के 1000 चिट्ठों (जिनके पीछे मुश्किल से 250 चिट्ठाकर हैं) में दो तीन ध्रुवीकरण दिख रहे है. यह अच्छी बात नहीं है — शास्त्री जे सी फिलिप
आज का विचार: हिन्दी ही हिन्दुस्तान को एक सूत्र में पिरो सकती है.
इस विषय में मेरा और आपका योगदान कितना है??
बहुत सीधी सी बात है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तो सिर्फ़ नाम प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉगस्पाट, वर्डप्रेस डाट काम और अपनी होस्टिंग कम्पनी के कान्ट्रेक्ट को दोबारा पढकर देखे। मुझे पूरा यकीन है उसको पढने के बाद (और समझने के बाद) इन सभी साहबान को पूरी समझ आ जाएगी। यदि नही आयेगी तो सम्बंधित व्यवस्था उनसे स्वयं निबटेगी। हमे क्या!
हमे सिर्फ़ चिन्ता उस बात की है, भारत सरकार (जो अभी भी तकनीकी रुप से पैदल है) कंही ऐसे हिन्दी ब्लॉग देखकर सारे हिन्दी ब्लॉग्स पर प्रतिबन्ध की मांग ना कर दें। वैसे भी सरकारों के फरमान ऐसे ही होते है।
देबू बाबू, जीतू जी को समझाइए। इतिहास के अनगिनत पड़ावों पर बहाल की गयी पाबंदियों का हश्र क्या हुआ। अभिव्यक्ति के ये तकनीकी स्रोत, जिनकी चर्चा जीतू जी कर रहे हैं, अगर झाड़ू से सबको बुहार भी देंगे- तो क्या ऐसी अभिव्यक्ति को कोई दूसरी ज़मीन नहीं मिलेगी। भारत सरकार को छोड़िए। ये मूरख मन का बयान आपने दिया है। सरकारी दमन की लंबी फेहरिस्त के बावजूद सरकार के खिलाफ प्रतिरोध हर समय जारी रहता है। आप जैसे लोग सरकारी मोहताज के छाते में लिखते रहें- जिन्हें कोई छाता नहीं चाहिए, वे भी लिखते रहेंगे। भाषा में तमीज और तरतीब आदमी को खुद सीखने दीजिए। और यक़ीन मानिए, वही भाषा और कहन बचेगी, जो कायदे से कही जाएगी। सजावट से कही जाएगी। लय में कही जाएगी।
भाषा पर नियंत्रण जरूरी है….वर्ना ऐसा ना हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस खेल में ,खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलनें लगे और सभी उसी भड़ासी भाषा का इस्तमाल शुरू कर दे।
जीतू जी ने परंपरागत हड्कौआ वाला रुख यहां भी अपनाया है -उनसे यही अपेक्षित भी था ! देवाशीष की बातों में कई मुद्दे उठे हैं उनपर बहस बाद तक जारी रह सकती है क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के सही मायनों की खोज लगातार होती रहेगी !
यह लेख देख कर थोड़ा सकुन मिला. साधूवाद.
अविनाश बाबू,
वैसे तो मै किसी बहस मे पड़ना नही चाहता क्योंकि आप बहस मे मुद्दे से उठकर, व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते है। सिर्फ़ एक उदाहरण देना चाहता हूँ।
हिन्दी न्यूज चैनल हमारे देश में खबरों का स्त्रोत हुआ करते थे, टीआरपी, अभिव्यक्ति, जागरुकता और आम आदमी के समाचारों के नाम पर आजकल क्या परोसा जा रहा है उससे कुछ छिपा नही। टीआरपी की अंधी दौड़ ने चैनलो को (अपराध करके) खबरें बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। चैनलो ने सैल्फ़ सैंसरशिप की बात की, तब भी बात बनी नही। अब सरकार जल्दी ही इस पर एक बिल लाने वाली है, जिसमे भाषा और कन्टेन्ट की मर्यादा रखने की बात होगी। इससे कुछ घटिया चैनलों के साथ साथ कुछ अच्छे चैनल भी प्रभावित होंगे। आम आदमी तो अब तक न्यूज चैनल देखने से वैसे ही तौबा कर चुका है। बस वही हाल हिन्दी ब्लॉगिंग की दुनिया का ना हो।
बाकी भविष्य मे ही सब कुछ लिखा है। हम और आप सिर्फ़ भाषा की मर्यादा बनाए रख सकते है, वो भी यदि आप नही चाहते तो जो मर्जी मे आए करिए।
इस लेख को मैं आपका अब तक का सर्वश्रेष्ठ लेख कहूंगा क्योंकि कुछ लोग जो अपने पेशे से अध्यापक,पत्रकार और संवेदनशील लेखक है उनको शायद नये ब्लॉगरों का प्रतोरोध करने का साहस ही नहीं है ये बात आपने सच कही कि आप जो ब्लॉग पर लिखते है वो अपने जीवन में भी उतार पायें तो हम आपकी लेखनी को एक प्रेरणा समझेंगें लेकिन उनको डर है कि अगर वो अच्छा लिखेंगें तो उनके प्रशंसको की संख्या में गिरावट आयेगी जो उन्हें पसंद नहीं.
बहुत सधी हुई बात कही आपने, विचार के बाद हम यही सकते हैं कि सहमत!
साहित्य में भदेस भाषा के प्रयोग से सहमत होते हुए, जीतू भाई की इस बात से भी मैं सहमत होना चाहूंगा कि कहीं ऐसे ही भदेस भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के आधार पर ही कहीं सारे ब्लॉगमण्डल पर पाबंदी की नौबत ना आ जाए!
कल की बैठक में सवाल सीधा दागा था यशवंत पर – “क्या यार इरादे क्या हैं, योजना क्या है, पता भी है कि आप धुरी बन रहे हो और यह भी कि नारद विरोधी रवैया त्यागों मित्र , नारद अब विरोध करने लायक चीज नहीं है, संरक्षण लायक चीज हो गई है (ऐतिहासिक मान्यूमेंट टाईप)”. यशवंत की राय साफ थी कि भई लर्निंग प्रोसेस में है और ये भी कहा कि आप न जाने क्यों पढते हैं हमारे आर्गेट पाठक आप नहीं है वरन वे कस्बाई पत्रकार हैं जिनमें भड़ास भरी हुई है- शुचितावादी जहॉं चाहें जाएं। इस आत्मविवास व साफगोई के बाद इतना तो मानना ही होगा कि भाषा पर उनकी समझ के ठीक ठाक होने के पेशेवर आधार हैं, उनमें से अधिकांश पत्रकार हैं तथा भाषा से उनका नाता वैसे ही है जैसे कि बढई का रंदे से होता है।
वैसे किसी नए ब्लॉगर मित्र ने कहा, “भड़ास और नारद में ज्यादा अन्तर नहीं है. दोनों की भाषा अलग है लेकिन असहमति के लिए दोनों के पास कोई जगह नहीं है. नारद वाले माँ… ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, भडास वाले करते हैं. इसके सिवा दोनों 1 जैसे हैं, जिसकी बात उनको अच्छी नहीं लगती वो विरोधी है. भड़ास वालों के लिए वो नारद वाला है, और नारद वालों के लिए वो भडास वाला।” इसलिए साफ है कि भड़ास और उससे असहमतियों दोनों का अपना लोकतांत्रिक स्पेस है जिसे वे इस्तेमाल कर रहे हैं। भड़ास के बाद राहुल शिष्ट दिखने लगे :))
वैसे स्त्रीवादी ब्लॉगिंग समुदाय ने भड़ास और बाकी लोगों की भाषा का विरोध किया तो है – शुचिता के आग्रह में नहीं पर स्त्रीविरोधी तेवर के लिए।
पर जाहिर है कि बहस जारी रहने वाली है।
मजा आ गया आपके विचार पढ़कर। सवाल वही है कि आखिर कब तक हम थोथे आर्दशों को अपने ऊपर ओढ़ते रहेंगे। क्यों हम दूसरे के पीछे-पीछे चलते रहना चाहते हैं।
जीतू जी, आप बात ही नहीं समझ रहे, तो कितना समझाया जाए।
एक बार फिर से वही बहस यहां होती दिख रही है। जब तक कोई सत्य कह रहा है, उसकी अभिव्यक्ति को पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि उसके सत्य कहने का तरीका अप्रिय या अशोभनीय हो तो यह सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वह उस अप्रिय सत्य को सुन-समझकर ग्रहण कर ले, या फिर नजरंदाज कर दे।
लेकिन यह बात हर किसी को याद रखनी होगी कि अभिव्यक्ति का चाहे जो भी माध्यम चुना जाए, उसकी स्वतंत्रता उस देश के संविधान और क़ानूनों के अध्यधीन ही होती है। यदि किसी की अभिव्यक्ति से देश के क़ानूनों का उल्लंघन होगा, तो उसे नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, चाहे वह कोई पत्रकार हो, कलाकार हो, ब्लॉगर हो या कोई अन्य नागरिक।
अपनी बात अच्छी तरह से कह ली। यशवंतजी ने कल बताया कि वो अपने ‘टारगेट पाठकों’ के लिये लिखते है। दूर-दराज के इलाके के पत्रकार उनके ‘टारगेट पाठक’ हैं। अविनाश से ज्यादा बात नहीं हो पायी लेकिन जितनी हो पायी उसमें मैंने कहा- मोहल्ले में बहस के चक्कर में अक्सर मामला खिच़ड़ी हो जाता है। समझ नहीं आता। उनका कहना था-जो खिच़ड़ी लगता है उसे आप इग्नोर कर दीजिये। इस सहज बात के बाद कुछ और कहने को रह नहीं जाता।
मुझे अच्छी तरह याद है कि जब तुमने कमेंट किया था मेरे ब्लाग की भाषा पर फिर उसके बाद मैंने पोस्ट लिखी थी तुम्हारी खिंचाई करते हुये। फिर तुमने कमेंट किया था जिसमें अपने कमेंट के लिये अफसोस जाहिर किया था। तुमको खराब लगा यह सोचकर मैंने तुमको मेल लिखी। फोन किया। ताकि अपना अफसोस जाहिर कर सकूं अपनी पोस्ट के लिये।
तो यह व्यक्ति के अपनी समझ के ऊपर है कि वो किसी चीज को कैसे लेना चाहते है। अपने विचार के अनुसार तर्क भी गढ़ लिये जाते हैं। तर्क शास्त्रियों की आउटसोर्सिंग भी होती है भाई!
वैसे ये भी एक रंग है। हर तरह के रंग आ रहे हैं। ब्लागिंग रंग-बिरंगी हो रही है। सही है। लगे रहो। बाकी फिर कभी!
बहुत सुन्दर लेख। बाकी साधारण सा नियम है कि:
सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यं अप्रियम।
bhayi…maine aaj syber cafe me baith kar ye past n comments padhe. mera jo computer tha, uspe devashish ke blog ke shabd agdam-bagdam dikhte hai.
Debu ji, aapko baaten prabhawshali hain lekin hawa-hawayi hain…. aap ki sochdaani ki apni simaayen hain. lekin debate start karne ke liye saadhuwaad. es post n comments ko mai bhadas pe daalen jaa reha hu. jidhar baitha hu udhar hindi type karne ke pryas me ek-do ghante kharch karne ki bajay maine roman mi likhna jyaada uchit samjha. ummid hai aap maaf karenge aur blogs ke baare me essi tarah likhte rahenge. mera propsal hai ki aap ek saptahik column apne blog pe shuru kariye, blogo me andarkhane chal rahi dhamachaukdi ke upar…
thanks n regards
yashwant